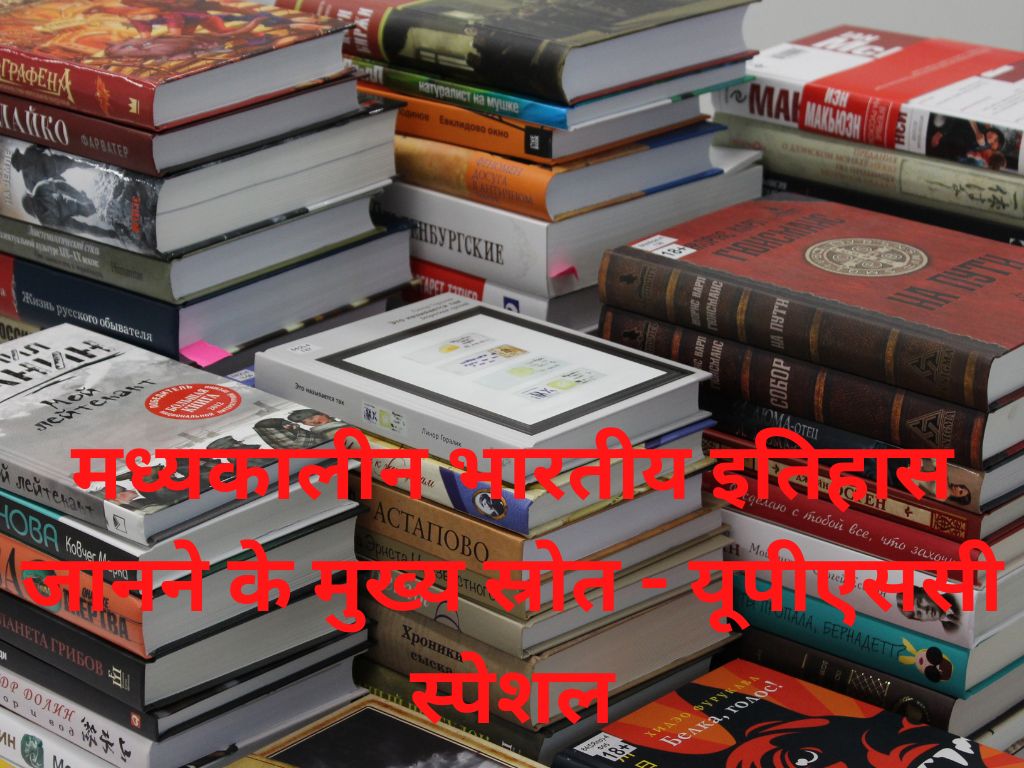
मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के मुख्य स्रोत – यूपीएससी स्पेशल– वे साधन जो अतीत की घटनाओं की जानकारी देते हैं, ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए मुख्यतः साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। इस लेख में हम आपके लिए मध्यकालीन साहित्य की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
इस्लाम-पूर्व काल में अरबों में वंशावलियाँ लिखने की परम्परा विकसित हुई, जिसे ‘अंसब’ कहा जाता था।
अरबों ने ‘यस्मा उल-रिजाल’ नामक कार्यों की एक नई श्रेणी पेश की, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की संक्षिप्त जीवनी संकलित की गई थी।
- ‘सीरत’ हजरत मुहम्मद की जीवनी का संकलन है।
- युद्धों का लेखा-जोखा ‘मगाजी’ के रूप में संकलित किया गया।
- ‘तबकात’ सामान्य इतिहास से संबंधित है। जिसमें विभिन्न समुदायों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- प्रशंसा के लिए मनाकिब और फैजल शब्द का प्रयोग किया जाता था।
- बदरुद्दीन द्वारा रचित ‘शाहनामा’ मुहम्मद तुगलक को समर्पित एक श्रद्धांजलि है।
- शमसे सिराज अफीफ की ‘तारीख-ए-फिरोजशाही’ नैतिक उपदेश प्रदान करने वाली पहली रचना है।
मध्यकालीन इतिहास के ज्ञान के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं।
1– चचनामा (सिंधी: चचनामो चचनामो)-, सिंध के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। इसमें चाच वंश के इतिहास और सिंध पर अरबों की विजय का वर्णन है। इस पुस्तक को ‘फतनामा सिंध’ (सिंधी: فتح نامه سند) और ‘तारीख अल-हिंद वास-सिंध’ (अरबी: تاريخ الهند والسند) भी कहा जाता है। चाच राजवंश ने राय वंश के अंत के बाद सिंध पर शासन किया। यह एक अज्ञात लेखक द्वारा अरबी में लिखा गया है। अबुबकर कुफी नसीरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। यह किताब बताती है कि खलीफा वाहिद ने मुहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा दी थी।
2 – तहकीक-ए-हिंद (किताब-उल-हिंद) – इसकी रचना अलबरूनी ने अरबी भाषा में की थी। अलबरूनी एक महान विद्वान था। भारत में रहते हुए उन्होंने एक विषय के रूप में संस्कृत का बहुत शौक से अध्ययन किया और हिंदू दर्शन और अन्य शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया। इसमें 1017-1030 के बीच भारत की स्थिति का वर्णन है। अलबरूनी का जन्म 973 ई. में खिवा (मध्य एशिया) में हुआ था। वह गजनी के महमूद के साथ भारत आया था।
इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने ‘तहकीक-ए-हिंद’ (भारत की खोज) नामक ग्रंथ की रचना की।
इस ग्रंथ में हिन्दुओं के इतिहास, चरित्र, आचरण, परम्पराओं और वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार से वर्णन किया गया है।
सचाऊ ने सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी भाषा में ‘अल्बरूनी इंडिया, एन अकाउंट ऑफ द रिलिजन’ नाम से अनुवाद किया।
इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत वर्मा ने किया है।
3- ताज-उल-मासीर नाम की इस किताब की रचना ‘सदरुद्दीन मुहम्मद हसन निजामी’ ने की थी। यह अरबी भाषा में है। इसमें 1192 ई. से 1228 ई. तक की अवधि की घटनाओं का वर्णन है। हसन निजामी इस ग्रंथ में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन और शासन काल तथा इल्तुतमिश के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों का वर्णन किया गया है। इतिहासकार इलियट और डॉसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है।
निजामी के अनुसार दिरहम और दिनार नामक सिक्के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा चलाए जाते थे।
4- तबक़ात-ए-नासिरी (फ़ारसी: طباقت ناسری) एक इतिहास की किताब है जो फ़ारसी भाषा में है। तबकात-ए-नसीरी की किताब ‘मिनहाजुद्दीन सिराज’ (1193-1254) (मिनहाजुद्दीन अबू-उमर-बिन सिराजुद्दीन अल-जुजियानी) द्वारा रचित है।
- इस ग्रंथ में मुहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के लगभग 1260 ई. तक के प्रारम्भिक इतिहास की जानकारी मिलती है।
- मिन्हाज ने यह पुस्तक अपने संरक्षक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की।
- मिन्हाज उस समय दिल्ली का प्रमुख काजी था।
- इस किताब में 1227-1259 तक का इतिहास है।
- मिन्हाज नसीरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि थे।
5- तारीख-ए-फिरोजशाही (फारसी भाषा) के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। बरनी का जन्म 684 हिजरी संवत में बलवन के शासनकाल में हुआ था। यह 1285-86 ई. में हुआ था। इसमें बलवन के राजगद्दी पर बैठने का इतिहास 1265 ई. से लेकर फिरोजशाह के छठे वर्ष तक लिखा गया है। जियाउद्दीन बरनी ने अपनी पुस्तक में राजस्व की स्थिति का बहुत विस्तार से वर्णन किया है।
6-फतवा-ए-जहाँदारी – जियाउद्दीन बरनी को इस कृति के रचयिता के रूप में जाना जाता है। इस पुस्तक में बरनी द्वारा अलाउद्दीन के अनेक आर्थिक सुधारों और सिद्धांतों को लिखा गया है। भारत कार्यालय के पुस्तकालय में फतवा-ए-जहाँदारी की केवल एक हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। इसमें 248 पृष्ठ हैं। कहीं बीच के पन्नों को मिटा दिया गया है। बरनी ने इस ग्रंथ में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा है। लेकिन “दुआगोई सुल्तानी” सुल्तान का दयालु शब्द है जो लेखक के लिए लिखा गया है।
7- तारीख-ए-फिरोजशाही-अफीक का पूरा नाम ‘शम्स-ए-सिराज अफीक’ था। वह फारसी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान लेखक थे।
- तुगलक सुल्तान फिरोज शाह ने आफीक को संरक्षण दिया।
- आफीक ने अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें केवल तारीख-ए-फिरोजशाही उपलब्ध है। उसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था।
8-सीरत-ए-फिरोजशाही – यह एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित ग्रन्थ है। यह पुस्तक सुलतान फिरोजशाह के समय में लिखी गई।
9- फतुहात-ए-फिरोजशाही – यह सुल्तान फिरजशाह तुग़लक़ की आत्मकथा है। इस ग्रन्थ में फ़िरोशाह द्वारा किये गए धर्मार्थ कार्यों का उल्लेख है।
10- फुतुह-उस-सलातीन- इस ग्रन्थ के लेखक ख़्वाजा अब्दुल्लाह मलिकइसामी है। यह ग्रन्थ बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमनशाह के संरक्षण में 1250 में पूर्ण हुई। इसमें 999 से 1350 तक का इतिहास वर्णित है।
11- क़ामिल-उत-तवारीख – इसका लेखक शेख अब्दुल हसन (इब्नुल असीर) है। इसमें मुहम्मद ग़ोरी की विजय का वर्णन मिलता है।
12- तारीख-ए -सिंध या तारीख-ए-मासूमी – इसकी रचना मीर मुहम्मद मासूम ने की थी। इसमें अरबों की भारत विजय से लेकर मुग़ल सम्राट अकबर तक का इतिहास है। यह मुख्यतः चचनामा पर आश्रित है।
13- तारीख-ए-मसूदी – इस पुस्तक की रचना अबुल फजल मुहम्मद बिन हुसैन-अल-बैहाकि ने की। बेहाकि महमूद गजनबी का एक शाही लेखक था। उसकी एक अन्य पुस्तक तारीख-ए-सुबुक्तगीन है। लेनपूल ने इसे पूर्वीय श्रीपैपियस की उपाधि दी है।
14- तारीख-ए-यामिनी- इस पुस्तक का लेखक उत्बी है। इस पुस्तक में सुबक्तगीन और महमूद गजनबी का 1020 तक का इतिहास वर्णित है।
15- तारीख-ए-मुबारक़शाही– इसकी रचना यहिया-बिन-सरहिंदी ने मुबारक शाह ( सैयद वंश) के संरक्षण में की।
16– रेहला- इस पुस्तक की रचना इब्न बतूता ( शेख फतह अबू अब्दुल्लाह) ने की। वह एक अफ़्रीकी (मोरक्को ) यात्री था। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। मुहम्मद तुग़लक़ ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। वह 1333 में भारत आया और 14 वर्ष भारत में रहा।
17- मालफूजाअत-ए-तैमूरी– यह तुर्की भाषा में लिखित अमीर तैमूर की आत्मकथा है। सर्वप्रथम आबू तालिब हुसैनी ने इस पुस्तक का फ़ारसी में अनुवाद किया।
18- ज़फरनामा– इस पुस्तक को सारफ-उद्दीन-अली यज़ीद ने अमीर तैमूर के पुत्र के संरक्षण में लिखी।
19- वाकिया-ए-मुश्ताकी और तारीख-ए-मुश्ताकी – इन दोनों ग्रंथों की रचना शेख रिजाकुल्लाह ने की।
20- तारीख-ए-सलातीन-ए-अफगान– यह अहमद यादगार की रचना है। इसमें बहलोल लोदी से लेकर हेमू तक का इतिहास है।-https://www.onlinehistory.in
21- मुखजान-ए-अफगानी– इस पुस्तक की रचना 1612 ईस्वी में नियामत उल्लाह ने की। यह लोदी वंश से संबंधित है।
22- अदाबुल-हर्ब-शुजाअत- इसका लेखक फख-मुदब्बिर है। यह इल्तुतमिश को समर्पित है।
23- इंशाए माहरु- यह पुस्तक तुग़लक़ काल में मुल्तान के प्रान्तपति ऐनुल-मुल्क के पत्रों का संकलन है।
24- रियाजुल इंशा– बहमनी सल्तनत बजीर महमूद गंवाँ के पत्रों का संकलन।
25- तारीख-ए-रशीदी– मिर्जा हैदर द्वारा लिखित ग्रंथ। कश्मीर का इतिहास।
26- रियाज-ए-सलातीन– इसका लेखक गुलाम हुसैन सलीम है। बंगाल का इतिहास।
27- तारीख-ए-गुजरात– मीर अबू तुरबवली द्वारा रचित।
28- आमिर खुसरो की पुस्तकें– यह तूती-ए-हिन्द के नाम से मशहूर है। अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर ख़ुसरो (1253-1325) चौदहवीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे।
उसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में हुआ था। खुसरो की माँ बलबन के युद्धमंत्री इमादुतुल मुल्क की पुत्री तथा एक भारतीय मुसलमान महिला थी। सात वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहान्त हो गया। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारम्भ किया और २० वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए।अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था।
- वह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था।
- निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दी।
- वह प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया।
- वह खड़ी बोली का अविष्कारक माना जाता है।
अमीर खुसरो की पुस्तकें
किरान-उस-सदायन
ऐतिहासिक विषय पर उनकी पहली रचना “किरान-उस-सादेन” है जिसे उन्होंने 1289 ई. में लिखा था। इसमें बुगरा खान और उनके पुत्र कैकुबाद की मुलाकात का वर्णन है। इसमें दिल्ली, इसकी इमारतों, शाही दरबार और रईसों और अधिकारियों के सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प विवरण शामिल हैं। इस रचना के माध्यम से उसने मंगोलों के प्रति अपनी घृणा भी व्यक्त की।
मिफ्ता-उल-फुतुह
उसने 1291 ई. में मिफ्ता-उल-फतुह की रचना की। इस रचना में उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों, मलिक छज्जू के विद्रोह और उसके दमन, सुल्तान के रणथम्भौर पर आरोहण तथा अन्य स्थानों की विजयों का विचार किया है।
खाजाइन-उल-फतुह
खजैन-उल-फुतुह, जिसे तारिख-ए-अलाई के नाम से भी जाना जाता है, में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के पहले 15 वर्षों का एक चापलूसी भरा लेखा-जोखा है। यद्यपि यह कृति मूलतः साहित्यिक है, तथापि इसका अपना महत्व है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन विवरण इसी ग्रंथ में मिलता है।
इसमें उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात, चित्तौड़, मालवा और वारंगल की विजय के बारे में लिखा है। इसमें हमें मलिक काफूर के दक्कन अभियानों का चश्मदीद गवाह मिलता है, जो भौगोलिक और सैन्य विवरण की दृष्टि से काफी प्रसिद्ध हैं। इसमें अलाउद्दीन के भवनों और प्रशासनिक सुधारों के वर्णन के साथ-साथ भारत का बहुत अच्छा चित्रण है। परन्तु अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल पर विचार करते हुए उसकी दृष्टि आलोचनात्मक नहीं रही है।
आशिका
अमीर खुसरो की “आशिका” की एक अन्य रचना गुजरात के राजकरन की पुत्री देवलारानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्रखान की प्रेम कहानी से संबंधित है। इसमें गुजरात और अल्वा में अलाउद्दीन की विजय की चर्चा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृति का भी वर्णन किया है। इसमें वह मंगोलों द्वारा अपने स्वयं के कारावास की बात भी करता है।
नूह सिपिर
एक और किताब जहां हिंदुस्तान और उसके लोगों को अच्छी तरह से चित्रित किया गया है, वह नूंह सिपिहर है। इसमें मुबारक खिलजी का बड़ा ही मनोहर वर्णन है। मुबारकशाह के भवनों की विजयों के साथ-साथ उन्होंने जलवायु, शाक, फल, भाषा और जीवन दर्शन जैसे विषयों पर विचार किया है। इसमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति का अत्यंत सजीव चित्रण देखने को मिलता है।https://www.historystudy.in/
तुगलकनामा
तुगलकनामा खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। इसमें ख़ुशरोशाह के खिलाफ गयासुद्दीन तुगलक की जीत को दर्शाया गया है। पूरी कहानी को धार्मिक रंग में पेश किया गया है। इसमें गयासुद्दीन सत् तत्वों का प्रतीक है और उसे असत्य तत्वों को लेकर अमीर खुसरोशाह से लड़ते हुए दिखाया गया है।
अमीर खुसरो का एक मजबूत पहलू यह है कि उन्होंने कई तारीखें दी हैं और उनके द्वारा दिया गया कालक्रम बरनी की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। उनकी रचनाएँ समकालीन सामाजिक परिस्थितियों पर भी बहुत प्रकाश डालती हैं और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर उस समय के अन्य इतिहासकारों ने अधिक ध्यान नहीं दिया।
