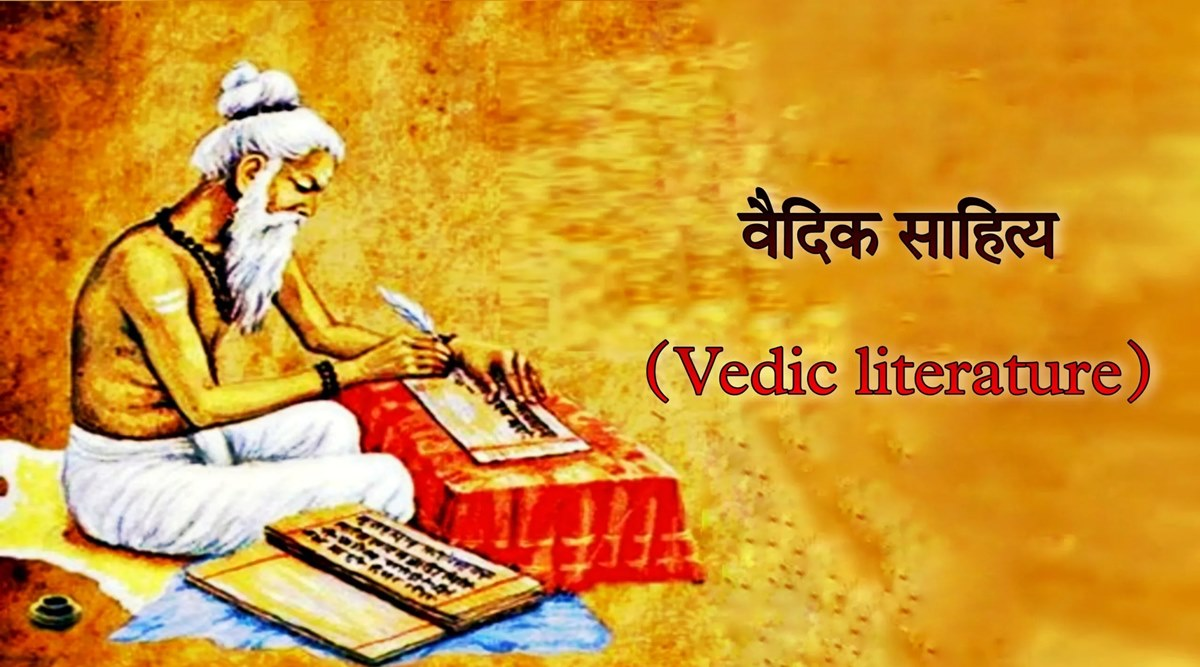हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात् भारत में एक नवीन सभ्यता का उद्भव हुआ और इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के बारे में सबसे ठोस जानकारी वेदों में मिलती है जिसके कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यद्यपि प्रारम्भ मरण वेद मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। वेद लिखित रूप में कब सामने आये इसके बारे में कोई ठोस अथवा प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ध्यातव्य है कि वैदिक सभ्यता का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता। इस लेख में हम वैदिककालीन साहित्य जैसे चार वेद, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बारे में जानेंगे।

वैदिककालीन साहित्य
वैदिक साहित्य का सामान्य अर्थ अगर माने तो इसके अंतर्गत चार वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद से है। उपवेद क्योंकि काफी बाद में रचे गए इसलिए वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति के नाम से जाना जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनकर लिखा साहित्य। वेदों को औपौरुष्य और नित्य माना जाता है यानि वेदों में जो ज्ञान है वह देवताओं ने ऋषियों को प्रदान किया और ऋषियों ने अगली पीढ़ी के ऋषियों को दिया और यह क्रम तब तक चला जब तक कि वेद लिखित रूप में सामने नहीं आये। प्रथम तीन वेद ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। अथर्वेद चूँकि यज्ञों से इतर भौतिक जीवन से संबंधित है इसलिए इसे वेदत्रयी श्रेणी में नहीं रखा जाता।
ऋग्वेद- सबसे प्राचीन वेद
वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। यहाँ ऋक का अर्थ होता है छन्दोवद्ध रचना या मन्त्र [श्लोक] .ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को समर्पित मन्त्र और भाव भरे गीत हैं और इसमें भक्तिभाव की प्रधानता है। हालाँकि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के भी सूक्त हैं परन्तु प्रमुख रूप से देवताओं को समर्पित स्त्रोतों या मन्त्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद की रचना सप्तसैंधव प्रदेश में हुई जो अब आधुनिक पंजाब के अंतर्गत आता है।
ऋग्वेद में 10 मण्डल, 1028 सूक्त या [1017 सूक्त] एवं 10580 मन्त्र हैं। मन्त्रों को ऋचा भी कहा जाता है। सूक्त का अर्थ है ‘अच्छी उक्ति’ . प्रत्येक सूक्त में तीन से सौ तक मन्त्र या ऋचाएं हो सकती हैं। वेदों का संकलकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। इसीलिए इनका एक नाम वेदव्यास भी है।
ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र देवताओं को समर्पित हैं। ऋग्वेद के मन्त्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ सम्पन्न करता था उसे ‘होता’ कहा जाता था। ऋग्वेद के तीन पाठ हैं —
| 1 | साकल | 1017 सूक्त |
| 2 | बालखिल्य | इसे आठवें मण्डल का परिशिष्ठ माना जाता है। इसमें कुल 11 सूक्त है। |
| 3 | वाष्कल | इसमें कुल 56 सूक्त हैं परन्तु यह उपलब्ध नहीं हैं। |
ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। पहला, आठवां, नौवां और दसवां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। दसवां मण्डल, जिसमें पुरुष सूक्त भी है सबसे बाद में जोड़ा गया है, यहाँ हम सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक मंडल और उससे संबंधित ऋषियों की तालिका दी गई है —
| मण्डल | संबंधित ऋषि का नाम |
| प्रथम | मधुछन्दा, दीर्घतमा और अंगीरा |
| द्वितीय | गृत्समद |
| तृतीय | विश्वामित्र [गायत्री मन्त्र का उल्लेख है] |
| चतुर्थ | वामदेव [कृषि संबंधित प्रक्रिया] |
| पंचम | अत्रि |
| छठा | भरद्वाज |
| सातवां | वशिष्ठ |
| आठवां | कण्व ऋषि [इसी में 11 सूक्तों का बालखिल्य परिशिष्ट माना जाता है] |
| नौवां | पवमान अंगिरा [सोम का वर्णन] |
| दसवां | क्षुद्रसूक्तिय, महासूक्तिय |
| वेद | ब्राह्मण |
| ऋग्वेद | ऐतरेय तथा कौषीतकी |
| यजुर्वेद | शतपथ ब्राह्मण [कृष्ण यजुर्वेद], |
| सामवेद | ताण्ड्य/पंचविश और जैमिनीय |
| अथर्ववेद | गोपथ |
ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई इस विषय में विद्वानों में मतभेद है।
बाल गंगाधर तिलक– बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर वैदिक सभ्यता का प्रारम्भ 6000 ईसा पूर्व माना है।
याकोबी- याकोबी ने वैदिक सभ्यता के प्रारम्भ का समय ईसा पूर्व 4500 से ईसा पूर्व 2500 निर्धारित किया है।
मैक्स मूलर- मैक्स मूलर ने ऋक संहिताओं का काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निश्चित किया है।
विंटरनित्ज़- आधुनिक विद्वान विंटरनित्ज़ ने अनुसार वैदिक काल का समय ईसा पूर्व 3000 से माना है। विंटरनित्ज़ ने इसके पक्ष में कहा है कि भारत का ऋग्वेद और ईरान का अवेस्ता लगभग एक ही समय का है।
जिस समय वेदों का उद्भव हुआ उस काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, अपने गुरु से सुनकर याद किया हुआ यह साहित्य लगभग तीन हज़ार साल तक यथावत विद्यमान है। इसे लिखित रूप बहुत बाद में दिया गया।
ब्राह्मण ग्रंथ
वेदों को भलीभांति समझने के लिए ब्राह्मण गांठों की रचना हुई। इनकी रचना गद्य में हुई है। ऐतरेय तथा कौषीतकी ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं।
ऐतरेय ब्राह्मण- महिदास को ऐतरेय ब्राह्मण का संकलनकर्ता माना गया है। उनकी माता का नाम ‘इतरा’ था। इतरा पुत्र होने के कारण वे महिदास ऐतरेय कहलाए। इसी कारण उनके द्वारा रचित ब्राह्मण ऐतरेय-ब्राह्मण के नाम से जाना गया। इस ब्राह्मण में राज्याभिषेक के अवसर पर होने वाले विधि-विधानों का वर्णन मिलता है। इसमें सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन तथा शुनः शेप आख्यान है। ऐतरेय ब्राह्मण में अथाह, अनन्त जलाधि और पृथ्वी को घेरे समुद्र का वर्णन मिलता है।
यह भी पढ़िए– वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की खोज” – एक व्यापक विश्लेषण
कौषीतकी ब्राह्मण– कौषीतकी ब्राह्मण के रचयिता कुषीतक ऋषि थे। कौषीतकी अथवा शांखायन ब्राह्मण में विभिन्न यज्ञों का वर्णन मिलता है।
आरण्यक- आरण्यक का अर्थ ऐसा साहित्य जिसकी रचना वनों में हुई है तथा इन्हें वन-पुस्तक भी कहा जाता है। ये ग्रन्थ मुख्यतः वनों में रहने वाले सन्यासियों और स्नातकों के लिए लिखे गए हैं। ये ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश अथवा परिशिष्ट हैं। इनमें दार्शनिक सिद्धांतों और रह्स्य्वाद का वर्णन मिलता है। आरण्यक कर्मयोग [जो ब्राह्मणों का प्रमुख प्रतिपाद्य है] तथा ज्ञानमार्ग [जिसका उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है] के बीच सेतु का काम करते हैं।
ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं ऐतरेय व कौषीतकी।
उपनिषद- उपनिषद शब्द दो शब्दों के योग से बना है- उप+निष्। उप का अर्थ है निकट और निष् का अर्थ है बैठना। अर्थात वह ज्ञान जिसमें छात्र अपने गुरु के निकट बैठकर ग्रहण करते करते हैं। ये वेदों के अंतिम भाग हैं। अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण 10 ही माने जाते हैं और इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। ये 10 मुख्य उपनिषद इस प्रकार हैं- ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, माण्डूक्य, छान्दोग्य, वृहदरण्यक, ऐतरेय एवं तैत्तिरीय। उपनिषदों में मुख्तयः आत्मा और ब्रह्म का वर्णन है।
ऋग्वेद के दो उपनिषद ऐतरेय और कौषीतकी हैं।
यजुर्वेद
यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञीय विधि-विधानों से संबंधित है। यह गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें कुल 1990 मन्त्र संकलित हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को ‘अध्वर्यु’ कहा जाता है। यजुर्वेद दो शाखाओं में विभाजित है- शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद- इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यह दो शाखाओं काण्व और मध्यदिन में विभाजित है।
कृष्ण यजुर्वेद- यह चार शाखाओं में विभाजित है यथा- काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता, और तैत्तिरीय संहिता। कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्रों की व्याख्या गद्य रूप में मिलती है।
ब्राह्मण ग्रन्थ
शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य को इसका लेखक माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में जल-प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा-उर्वशी आख्यान, रामकथा तथा अश्वनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन मिलता है।
कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है।
आरण्यक– यजुर्वेद के आरण्यक वृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ हैं।
उपनिषद- यजुर्वेद के उपनिषद में प्रमुख रूप से वृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद ईशोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद एवं महानारायण उपनिषद हैं।
वृहदारण्यक उपनिषद में में याज्ञवल्क्य-गार्गी का प्रसिद्ध संवाद, तैत्तिरीय उपनिषद में ‘अधिक अन्न उपजाओ’ एवं कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है। इस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है।
सामवेद
भारतीय संगीत के उद्भव का पहला बीज सामवेद में ही है। साम का अर्थ है गायन। सामवेद में कुल मन्त्रों की संख्या 1549 है। इन मन्त्रों में सिर्फ 75 ही मौलिक मन्त्र है। शेष ऋग्वेद से ग्रहण किये गए हैं। अतः इसे ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है।
सामवेद में मन्त्रों को गाने वाले ऋषि को उद्गाता कहा गया है। सात सुरों का सर्वप्राचीन उल्लेख सामवेद में ही मिलता है- सा…….रे…….गा…..मा। सामवेद की मुख्यतः तीन शकाहें हैं – कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय।
ब्राह्मण ग्रन्थ- मूल रूप से सामवेद के दो ब्राह्मण हैं- ताण्ड्य और जैमिनीय। ताण्ड्य ब्राह्मण बहुत बड़ा है इसीलिए इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। यह 25 अध्यायों में विभक्त है। इसीलिए इसे पंचविश भी कहा जाता है। षड्विष ब्राह्मण, ताण्ड्य ब्राह्मण के परिशिष्ट के रूप में है, इसे ‘अदभुत’ ब्राह्मण भी कहा जाता है।
जैमिनीय ब्राह्मण में याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन है।
आरण्यक- इसके दो आरण्यक हैं- जैमिनीय आरण्यक व छन्दोग्यारण्यक।
उपनिषद- सामवेद के दो उपनिषद हैं- छान्दोग्य उपनिषद एवं जैमिनीय उपनिषद। छान्दोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। देवकी पुत्र श्रीकृष्ण का सर्व प्रथम उल्लेख इसी में है। इसमें प्रथम तीन आश्रमों तथा ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि एवं उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच विख्यात संवाद का वर्णन है।
यह भी पढ़िए– उपनिषद: उपनिषद का अर्थ, महत्व और उपयोगिता
अथर्ववेद
अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका एक नाम ‘अथर्वांगिरस’ भी पड़ गया। अथर्व शब्द अथर+वाणी शब्दों के संयोजन से बना है। इसका तात्पर्य है जादू टोना। कुछ विद्वान अथर्वन का वास्तविक अर्थ अग्नि उद्बोधन करने वाला पुरोहित मानते हैं। किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद ही करता है। अतः इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद के मन्त्रों का उच्चरण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। चारों वेदों में यही वेद सबसे लोकप्रिय है। अथर्ववेद गद्य और पद्य दोनों में है।
अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मन्त्र हैं। अथर्ववेद में जादू, टोन, वशीकरण, बीमारी दूर करने वाले मन्त्र आदि का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार अथर्ववेद जनसामान्य के अन्धविश्वास और दैनिक क्रिया कलापों का लेखा जोखा है। इसके अधिकांश मन्त्र दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्त होने के लिए हैं।
अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया है। इसी में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है।
अथर्ववेद की दो शाखाएं शौनक और पिप्पलाद हैं।
ब्राह्मण- अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ है। जिसका संकलनकर्ता गोपथ ऋषि को माना गया है।
आरण्यक– अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है।
उपनिषद- इसके प्रमुख उपनिषदों में मुण्डकोपनिषद, माण्डूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद हैं।
भारत का प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते मुण्डकोपनिषद से ही ग्रहण किया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी-फूटी नौकाओं से की गई है। अतः यज्ञों से जीवन रुपी नौका को पार नहीं किया जा सकता। सभी उपनिषदों में मुण्डकोपनिषद सबसे छोटा है।
निष्कर्ष
इस प्रकार वैदिक साहित्य हमारे हिन्दू धर्म और संस्कृति का मूल आधार है। अफ़सोस कि हमारे वर्तमान समाज में समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ और हम अपने मौलिक साहित्य को भूलकर बनाबटी और राजनितिक स्वार्थ से ग्रसित होकर हिंसक प्रवृत्ति को अपना रहे हैं जबकि हमारा मौलिक धर्म समानता, शांति और सहयोग का धर्म है। धर्म को समझने के लिए वेदों का अध्ययन पाली शर्त है। मगर वर्तमान में धर्म को जीवन जीने की पद्धति से ज्यादा लोगों को भड़काने और उन्हें हिंसक बनाने के लिए किया जा रहा है।