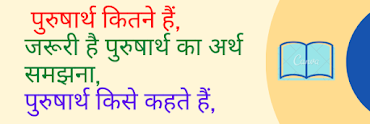पुरुषार्थ किसे कहते हैं?-जरूरी है पुरुषार्थ का अर्थ समझना,
पुरुषार्थ-का अर्थ
प्राचीन हिंदू ऋषि-मुनियों अर्थात हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया उन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। पुरुषार्थ का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से है यह मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं, उन्हें नियमित बनाते हैं तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित भी करते हैं।
पुरुषार्थों का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के बीच सामजस्य स्थापित करना है। भारतीय परंपरा भौतिक सुखों को क्षणिक मानते हुए भी उन्हें पूर्णतया तिरस्कृत या त्याज्य नहीं समझती, बल्कि उनके प्रति अतिशय आसक्ति का ही विरोध करती है। मनुष्य भौतिक सुखों के संयमित उपभोग द्वारा ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। भौतिक सुखों को आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में साधक माना गया है, बाधक नहीं। दोनों घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों का समन्वित स्वरूप पुरुषार्थों के माध्यम से प्रतिपादित या व्याख्यायित किया गया है।
पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं?
पुरुषार्थ चार प्रकार के हैं अर्थात- धर्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष। इनमें अर्थ तथा काम भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति में शेष पुरुषार्थ सहायक हैं। मोक्ष की प्राप्ति सभी के लिए संभव नहीं है। अतः कालांतर में तीन पुरुषार्थ धर्म अर्थ तथा काम के पालन पर ही बल दिया गया। इन्हें ‘त्रिवर्ग’ कहा गया है जिनकी प्राप्ति सभी ग्रहस्थों के लिए सरल है। हिंदू शास्त्र विधाओं का यह मत है कि तीनों पुरुषार्थ में कोई विरोध नहीं है तथा इनका पालन एक साथ हो सकता है। मानव जीवन का पूर्ण विकास तभी संभव है जब कि सभी पुरुषार्थों का सम्यक रूप से पालन किया जाए।
हिन्दू धर्म में मुख्य स्थान रखने वाले चारों पुरुषार्थों को विस्तार से जानते हैं
१- धर्म- धर्म पुरुषार्थों की प्रथम सीढ़ी है जिसे हिंदू जीवन दर्शन में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। ‘धर्म’ शब्द ‘धृ’ धातु से निष्पन्न होता है जिसका शाब्दिक अर्थ धारण करना अथवा अथवा अस्तित्व बनाए रखना है। यह वह तत्व जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक है प्राचीन शास्त्रों में इसकी विशद व्याख्या मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है सभी को सुरक्षित रखता है। यह सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है-(धारणात् धर्ममित्याहुः धर्यो धारयते प्रजाः। यत्स्या संयुक्त स धर्म इति निश्चय:।।- कर्णपर्व १०९.५८.)। आगे बताया गया है कि धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की गई है जिससे सभी प्राणियों का हित होता है वही धर्म है-(प्रभवार्थम् च भूतानां धर्म प्रवचनम् कृतम्। – कर्णपर्व १०९.५८.)।
वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जिससे लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है। वह धर्म है।(यतोऽभ्युदय निःश्रेयस् सिद्धि स धर्म।)। प्राचीन साहित्य में आचार ( सदाचार ) को धर्म का लक्षण बताएं गया मनुस्मृति में धर्म के चार स्रोत कहे गए हैं- वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि अर्थात जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे।(वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः। एतत् चतुर्विध साक्षाद्धर्मस्य लक्ष्णम्।।(- मुनु० २.६.१२.)। प्राचीन शास्त्रकारों ने वेद, स्मृति आदि धर्म-ग्रंथों में जो कर्तव्य विहित हैं, उनके निष्ठापूर्वक पालन करने को ही धर्म बताया है। वस्तुतः धर्म से तात्पर्य आचरण की उस संहिता से है जिसके माध्यम से मनुष्य नियमित होता हुआ विकास करता है और अंततोगत्वा परम पद ‘मोक्ष’ की प्राप्ति कर लेता है।
प्राचीन हिन्दू धर्म से जुड़े प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन्हें देखने से स्पष्ट है कि यह एक व्यापक शब्द था जिससे भारतीय ऋषियों ने सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, व्यक्तिगत गुणों आदि सभी का समावेश कर लिया था। अंग्रेजी का ‘रैलीजन’ (Religion) शब्द इसका पर्याय नहीं हो सकता। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता, समाज के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता, तथा अंततोगत्वा जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता था। धर्म के आद्योपान्त मनुष्य के साथ रहने वाला तत्व है। धर्म को कहीं-कहीं कर्तव्यों का संग्रह भी माना गया है।
- यह भी पढ़िए – ऋग्वैदिक आर्यों का खान-पान
२- अर्थ- इस शब्द का अर्थ संकुचित रूप में धन अथवा संपत्ति लगाया जाता है किंतु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में यह व्यापक शब्द था जिसका तात्पर्य उन समस्त आवश्यक संसाधनों से था जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य- धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता है। इसकी परिधि में वार्त्ता तथा राजनीति को भी समाहित कर लिया गया था। कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य वार्त्ता के क्षेत्र हैं ( कृषि पशुपाल्यावाजिज्या च वार्त्ता )। राजनीति का संबंध राजशासन से है। अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह सुख-सुविधा का साधन है।
प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में इसे ‘परमधर्म’ कहा गया है जिस पर सभी वस्तुएँ निर्भर करती है। जिसके पास अर्थ नहीं है वह मृतक तुल्य है जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुख पूर्वक निवास करते हैं।
“धनमाहु: परम धर्म धने सर्वम् प्रातिष्ठितम्।
जीवन्ति धनिनो लोके मृता ये त्वधना।।”– उद्योगपर्व ७२.२३—२४.
अर्थ के अभाव में जीवन यापन असंभव है। बृहस्पति ने अर्थ को जगत् का मूल स्वीकार किया है ( धन मूल जागत् )। अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व निरूपित किया गया है।(अर्थ एव प्रधानः। अर्थमूलौ हि धर्मकामाविति।)। नीतिशतक में विवृत है कि जिसके पास धन है वही कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, गुणवान् है, वक्ता है तथा दर्शनीय है। सभी गुण धन में ही होते हैं।
“यस्यास्ति वित्त स नर: कुलीन: स पण्डितः स पण्डितः स श्रतुवान्गुणज्ञ:।
स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वेगुणाः काञचनमाश्रयन्ति।।”
किंतु अर्थ की महत्ता स्वीकार करते हुए भी हिंदू शास्त्रकारों ने उसे धर्म के अधीन बताया है तथा धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति पर बल दिया है। जो अर्थ, धर्म की हानि करता है वह अभीष्ट नहीं है। मनुस्मृति में स्पष्टत: कहा गया है कि धर्म विरुद्ध अर्थ तथा काम का त्याग कर देना चाहिए। आपस्तंब ने भी कहा है कि मनुष्य को धर्म अनुकूल सभी सुखों का उपभोग करना चाहिए। इस प्रकार भारतीय जीवन-दर्शन में अर्थ वहीं तक अभीष्ट है जहां तक वह धर्मसंगत हो।
- यह भी अवश्य पढ़िए – कपिल मुनि का सांख्य दर्शन
३- काम- मानव जीवन का तृतीय पुरुषार्थ काम था जिसका शाब्दिक अर्थ इंद्रिय सुख अथवा वासना से है। किंतु व्यापक अर्थ में इस शब्द से तात्पर्य मनुष्य की सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से है। महाभारत के अनुसार काम मन तथा हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों के विषयों से संयुक्त होने पर निःसृत होता है।(इन्द्रियाणां च पञ्चानाम् मनसो हृदयस्य च। विषये वर्तमानानां या प्रीतिरुप जायते। स काम इति बुद्धि कर्मणा फलमुक्तम्।।)। यह संसार की प्रथम एवं सुख प्रमुख प्रवृत्ति है। इसी के वशीभूत ही मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है, गृहस्थ जीवन के विविध आनंदो को भोगता है तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखता है।
हिंदू शास्त्र कारों ने मानव जीवन से में काम के महत्व को स्वीकार करते हुए उस पर धर्म का अंकुश लगाया तथा यह प्रतिपादित किया कि धर्मसंगत काम का आचरण ही व्यक्ति एवं समाज की उन्नति कर सकता है।
इसके विपरीत होने पर यह मनुष्य के पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। काम के निरंकुश आचरण से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। काम की तृप्ति न होने पर क्रोध तथा क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। मोह से स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रम से बुद्धिनाश तथा बुद्धिनाश से मनुष्य का पूर्ण विनाश हो जाता है।
(ध्यायतों विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते। संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।। क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृति विभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।। ।
इसी कारण कृष्ण अपने को सभी प्राणियों में धर्मयुक्त काम बताते हैं( धर्माऽविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ )। मत्स्य पुराण में कहा गया कि ‘धर्मरहित काम बन्ध्या पुत्र के समान है ( धर्महीनस्य कामार्थो बन्ध्यासुत समौ ध्रुवम )। महाभारत के अनुसार जो व्यक्ति धर्मविहीन काम का अनुसरण करता है वह अपनी बुद्धि को समाप्त कर देता है तथा कठिनाइयों में शत्रु द्वारा हंसी का पात्र बनाया जाता है।(धर्मार्थावभिसंत्यज्य संरम्भ योऽनुमान्मते। हसन्ति व्यसने तस्य दुर्हदो न चिरादिव।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म शास्त्रकारों ने धर्म संबंधित काम का आचरण किए जाने पर ही बल दिया है। इसी से व्यक्ति का सम्यक विकास संभव है। काम का उच्छृंखल आचरण व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए हानिकारक है।
४-मोक्ष- हिंदू विचारधारा में मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है जिसकी प्राप्ति सभी का परम साक्ष्य है। चार्वाक के अतिरिक्त अन्य सभी विचारधारायें इसे स्वीकार करती हैं। मोक्ष का अर्थ पुनर्जन्म अथवा आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। आत्मा अजर, अमर एवं परमात्मा का ही अंश है। शरीर बंधन का कारण है। संसार मायाजाल है। मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है तो सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाता है। ज्ञान भक्ति एवं कर्म मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। गीता में इनका समन्वय मिलता है।
उपनिषदों में मोक्ष संबंधित विचारधारा का सम्यक् विश्लेषण मिलता है। उपनिषद् व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा तथा जगत के सारभूत तत्व ब्रह्म का तादाम्य स्थापित करते हैं। यही मोक्ष की अवस्था है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में इंद्रिय तथा मन का संयम, सांसारिक भोगों से विरक्ति, संसार की अनित्यता का ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा हो। तत्पश्चात उसे किसी योग्य गुरु से वेदांत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए।
गुरु शिष्य को ‘तुम ही ब्रह्म हो’ ( तत् त्वम असि ) का बोध कराता है। अपने ऋषि गुरु की इस बात को ध्यान में रखते हुए दृढ़तापूर्वक उसका आचरण करते हुए व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार कर लेता है तथा इस अवस्था में उसे ‘अहं ब्रह्मास्मि’ अर्थात् मैं ही ब्रह्म हूँ की अनुभूति होती है। यही पूर्ण ज्ञान है तथा इसी को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के बाद जीवन के दुःखों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य परमानंद की प्राप्ति करता है।
प्रायः सभी भारतीय दर्शन अविज्ञा तथा अज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हैं। अतः मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान के बंधन को काट दे। गीता में कहा गया है कि काम-क्रोध से रहित, जीते हुए मन वाले ज्ञानी पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष स्वयंमेव प्राप्त हो जाता है। गीता ज्ञान के स्थान पर भक्ति को प्रधानता देती है तथा मोक्ष के लिए ईश्वर की कृपा को आवश्यक बताती है।
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करुंगा।(सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज्ज। अहं तवाम् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।)
जैन तथा बौद्ध दर्शन में भी अविज्ञा के विनाश को ही मोक्ष का उपाय माना गया है। जैन इसके लिए त्रिरत्नों ( सम्यक् दर्शन, ज्ञान तथा चरित्र) एवं बौद्ध अष्टांगिक मार्ग ( सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक्, कर्मान्त, आजीव, व्यायाम, स्मृति तथा समाधि ) का विधान प्रस्तुत करते हैं। मनुस्मृति में विहित है कि इंद्रिय विरोधी राग-द्वेष रहित तथा अहिंसा परायण व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। पुराणों में मोक्ष के लिए दया प्राणियों में समभाव, क्षमा, अक्रोध, सत्य, लोभ, मोह, काम आदि का त्याग आदि गुणों का आचरण आवश्यक बताया गया है।
- यह भी पढ़िए – वैदिक काल में स्त्री की दशा
इस प्रकार मोक्ष हिंदू जीवन दर्शन का चरम लक्ष्य था। ब्रह्मचर्य आश्रम से ही विद्यार्थी को इसका बोध हो जाता था तथा जीवनपर्यंत वह अपने समस्त क्रियाओं को इसी ओर नियोजित करता था। जीवन के अंतिम आश्रम से इस लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति होती थी। पुरुषार्थ हिंदू विचारधारा की अपनी व्यवस्था है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में सर्वथा अप्राप्य है।
पाश्चात्य संस्कृति जहां भौतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है वहां भारतीय संस्कृति में भौतिकता को महत्वपूर्ण मानते हुए भी आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी गयी हैं।
पुरुषार्थ के माध्यम से भारतीय मनीषियों ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, आसक्ति एवं त्याग के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया है। यहां काम तथा अर्थ साधन हैं जबकि धर्म एवं मोक्ष साध्य स्वरूप हैं। त्रिवर्ग में तीनों पुरुषार्थों का अन्योन्याश्रित संबंध है। इनमें धर्म की स्थिति सर्वोच्च है। अर्थ तथा काम का उचित उपभोग धर्म के माध्यम से ही संभव है।
मनुस्मृति में तीनों के समन्वय पर बल दिया गया है। तदनुसार ‘कुछ कहते हैं कि मनुष्य का लाभ धर्म तथा अर्थ में है’, ‘ कुछ के अनुसार यह काम तथा अर्थ में है, जबकि कुछ लोग केवल धर्म में ही मनुष्य का लाभ देखते हैं। किंतु वस्तु-स्थिति यह है कि मनुष्य का कल्याण तीनों पुरुषार्थों के समुचित समन्वय में ही निहित है।
कुल्लूक भट्ट जो मनुस्मृति के टीकाकार हैं का विचार है कि “लौकिक दृष्टि से अर्थ एवं काम महत्वपूर्ण हैं किंतु पारलौकिक दृष्टि से विचार करने पर मोक्ष ही एकमात्र अभीष्ट रह जाता है तथा अन्य पुरुषार्थ इसकी प्राप्ति में सहायक बन जाते हैं।”
निष्कर्ष
पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से है। मनुष्य तथा समाज के बीच के संबंधों की व्याख्या करते हुए उन्हें न्याय संगत बताते हैं। दोनों के उचित संबंधों पर प्रकाश डालते हैं तथा उनके अनुचित संबंधों को उजागर करते हैं, ताकि मनुष्य उनसे बच सके। वस्तुतः पुरुषार्थ मनुष्य एवं समाज एवं उनके अन्तर्सम्बन्धों के नियामक हैं। आश्रमों के द्वारा जीवन यापन करता हुआ व्यक्ति विभिन्न पुरुषार्थों के माध्यम से समाज एवं परिवार के प्रति उत्तरदायित्वों का पूर्ण निर्वाह करता है।
इस ब्लॉग के अन्य महत्वपूर्ण लेख अवश्य पढ़ें
1-भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण-
2-ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का खान-पान ( भोजन)